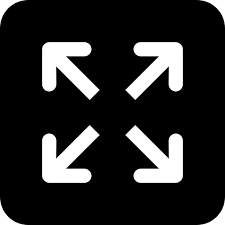TRENDING TAGS :
‘जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये’
 आनंद वर्धन
आनंद वर्धन
‘जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये’- गीतकार गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां कभी बचपन में पढ़ी थीं। शायद 45-46 साल पहले। तब ये ही समझ पाया था कि ये पंक्तियां केवल दीपावली जैसे त्योहार के लिए लिखी गई हैं पर बाद में इस कविता को पढऩे पर इसका अर्थ खुला। इसी कविता में नीरज आगे कहते हैं-
‘सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में
कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी
मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी
कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी
चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही
भले ही दिवाली यहां रोज आए’
दीपावली के आरंभ के पीछे कथा यह है कि असत्य पर सत्य की विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्या को दीपमालिका से सजाया गया। हर घर में उल्लास था कि राम के लौटने के बाद अब रामराज्य होगा। ऐसा रामराज्य जिसमें सभी सुखी हों और मनुष्यता का साम्राज्य चारों ओर होगा। राम भी आए, अयोध्या प्रफुल्लित भी हुई लेकिन कोई न कोई तो असंतुष्ट ही रहा।
आलोचक अपनी आलोचना से बाज न आए और सीता एक बार फिर निर्वासित हुईं। लोग दिवाली मनाते रहे और सीता को धरती की गोद में शरण लेनी पड़ी। अयोध्या के घी के दीपक सीता के जीवन में रामराज्य का सुख न ला सके। फिर भी सीता ने अपना शेष जीवन आत्माभिमान के साथ जिया।
दीपावली का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। हर्ष के नाटक नागानंद में इस उत्सव की चर्चा की गई है और इसे दीपप्रतिपादुत्सव: कहा गया है। राजशेखर काव्यमीमांसा में इसे दीपमालिका कहते हैं। यह त्योहार केवल हिन्दुओं का ही नहीं है बल्कि इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी मनाते हैं। साथ ही प्रवासी भारतीय भी धूमधाम से दीपावली मनाते हैं।
दीपक ज्ञान, सत्य और प्रकाश का प्रतीक है। वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह भारतीय परंपरा है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने को महत्व देती है। यह परंपरा निजता में नहीं बल्कि सार्वजनीनता में विश्वास रखती है जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए विचार करती है। यह भारतीय परंपरा ही है जो अंधकार को अज्ञान का प्रतीक मानती है और प्रकाश को ज्ञान और शक्ति का। कहा भी गया है-तमसो मा ज्योतिर्गमय।
आज यह तिमिरांधकार फैला हुआ है चारों ओर अशिक्षा, अज्ञान, भ्रष्टाचार, शोषण और दमन के रूप में। जहांं मनुष्यता का बोलबाला होना चाहिए वहां अमानवीयता अपने पैर पसार रही है। जिस समाज में उपलब्ध संसाधन सबके लिए होने चाहिए वहां सारा कुछ केवल कुछ लोगों के लिए हो, इस विचार की हिमायत की जा रही है। विद्रूपताओं का विस्तार हो गया है, धर्मांधता ने धर्म की व्याख्या बदल दी है और कर्मशीलता का महत्व कम हो चला है। अब हम यह सोचते हैं कि ईमानदारी तो हो पर दूसरे ईमानदार बने रहें हमारे लिए, हम ईमानदार नहीं होंगे।
स्वच्छता तो रहे पर हमारे दरवाजे पर और हम अपने घर का कूड़ा दूसरों के द्वार पर डालकर खुश हैं। जो भी संसाधन हों वे कुछ परिवारों के लिए रहें। यह भी मानसिकता बनती जा रही है कि प्रकाश केवल मेरे घर में हो और दूसरों का घर तिमिराछन्न रहे तो रहे। दिवाली आए तो बस मेरे यहां और घी के दिए जलें तो मेरे घर पर। दूसरों के घरों में मिट्टी के दीपक में तेल की बूंद भी न हो तो कोई बात नहीं।
वास्तव में भारतीय समाज बहुलतावादी है। वह एकवचन में विश्वास नहीं रखता और संयुक्तता को महत्व देता है। पहले जो परिवार संयुक्त थे वह सुखी थे। उन परिवारों के बच्चे आपस में खेलते-कूदते, लड़ते-झगड़ते और स्नेह करते न जाने कब बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। एक परिवार की तो बात ही क्या, मोहल्ले का हर परिवार एक बड़ी इकाई का हिस्सा होता था और पूरा का पूरा गांव एक इकाई के रूप में जाना जाता था।
किसी गांव के एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी मगर आज सबकुछ बदल चुका है। बाजार ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना ली है। जमीन पर बैठकर पंगत में खाने की परंपरा कम से कम उत्तर भारत के गांवों से तो समाप्त होती जा रही है। टेबल कुर्सी से भी आगे बढक़र बुफे प्रणाली में प्रीतिभोज आयोजित हो रहे हैं, लेकिन आज के प्रीतिभोज में प्रीति का भाव लुप्त है, दिखावट का अधिक।
क्या दीपावली की दीपमालिकाएं समाज के इस अंधकार को दूर कर पाएंगी? पता नहीं, लेकिन उत्सवधॢमता बनी रहनी चाहिए जो भारत की पहचान है। काॢतक अमावस्या की काली रात को प्रकाशमान बनाने का साहस हमारी संस्कृत में सदा से रहा है। लोक से जुड़ा हुआ यह त्योहार गांव के लिए रोजगार के अवसर लेकर आता है। बचपन में हम सारे बच्चे इनके साथ-साथ फुलझडिय़ों और अनार जैसे पटाखों का इंतजार किया करते थे। बहुत साल पहले तक ये पटाखे अक्सर स्थानीय लोग ही बनाते थे।
अब पटाखों के बड़े-बड़े कारखाने हैं और सारा व्यापार कुछ हाथों में केंद्रित है। खतरनाक रसायन हर साल अनेक जानें ले लेते हैं और महानगरों में दीपावली के पटाखों का धुआंं श्वसन रोगों के फैलने का कारण बन चुका है। मेले ठेलों में तमाम आधुनिकताओं के बाद भी थोड़ी बहुत ग्रामीण झलक मिल जाती है पर गंवई गांव गुलाब का जिस चालाकी के साथ बाजारीकरण हो रहा है और ब्रांडिंग की जा रही है उससे गांव का तो कोई खास लाभ होता नहीं दिखता।
दिवाली के अवसर पर या अन्य त्योहारों के अवसर पर दीवारों पर उकेरे गए चित्र और अल्पना गायब हो चले हैं। भविष्य में धीरे-धीरे ये अल्पनाएं सपने बन जाएंगी। फिर इन्हें देखने के लिए संग्रहालयों में जाना पड़ेगा या इन्हें शोध ग्रंथों में खोजना पड़ेगा। याद आती है रेणु की एक कहानी भित्तिचित्र की मयूरी की, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु लोक कलाओं के वैश्वीकरण की ओर संकेत करते हैं।
फूलपत्ती की मां और फूलपत्ती के हाथों में भारी हुनर है चित्रांकन का। वे प्रतीक हैं लोक की और सनातन नाम का शहरी साहब प्रतीक है बाजारीकरण का। फूलपत्ती की मां तमाम प्रलोभनों के बाद भी गांव छोडक़र नहीं जाती। यही है इस कहानी का चरमोत्कर्ष। रेणु ने बीच का रास्ता चुना है इस कहानी में पर लोक की विजय यहां भी है।
दीपावली के बहाने हम आज भी थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं अपने लोक को। यह भी कम बड़ी बात नहीं है। दीपावली फिर से आ गई है। अभी भी कुछ त्रिपुरासुर शेष हैं और शेष है उनके गण भी। वे फिर से नष्ट हों और सत्य का साम्राज्य स्थापित हो। मानवता फिर से सुखी हो, कहीं भी उदासी न रहे, तभी गीतकार नीरज की पंक्तियां सार्थक होंगी और सार्थक हो सकेगा-तमसो मा ज्योतिर्गमय।
(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय गांधी हिल्स, वर्धा-442005 (महाराष्ट्र) में प्रतिकुलपति हैं)