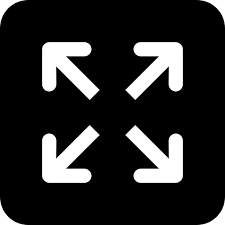TRENDING TAGS :
श्रीविष्णु प्रभाकर, जो चलते चले गये..उनकी जयंती पर मेरी कलम से
 आनंद वी ओझा
आनंद वी ओझा
प्रख्यात साहित्यकार स्व. विष्णु प्रभाकरजी की जयन्ती विशेष पर कुछ अंश.... सौभाग्य से मैं उनका स्नेहभाजन रहा हूं उन पर कुछ लिखने की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। जानता था, लिखने की बातें मेरे पास हैं, लेकिन यह स्मृति-लेख पूरा लिख न सका था। आज उस अकर्मण्ता से मुक्त होकर यह लंबा संस्मरण आप सबों के सामने रख रहा हूँ और इसी रूप में उनकी पावन स्मृतियों को स्मरण-नमन कर रहा हूँ।
सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रद्धेय विष्णु प्रभाकरजी के दर्शन का सौभाग्य पहली बार मुझे कब मिला था, यह स्पष्टतः स्मृति में अंकित नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि सन् 1971 में जब मैं पहली बार दिल्ली-दर्शन के लिए पिताजी के साथ वहाँ गया था और पिताजी अपने एक पुराने मित्र (जो दो वर्ष बाद ही उनके समधी भी बने) मार्तण्ड उपाध्यायजी से मिलने उनके दफ़्तर 'सस्ता साहित्य मण्डल, कनाॅट प्लेस जाने लगे तो मैं भी उनके साथ गया था; सम्भवतः विष्णु प्रभाकरजी के प्रथम दर्शन मुझे वहीं मिले थे। उनके एक-दो नितांत औपचारिक प्रश्नों के उत्तर देने के अतिरिक्त मेरी और कोई बात उनसे नहीं हुई थी। तब उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना और मेरा प्रणाम निवेेेेदित करना ही हुआ था। मार्त्तण्ड उपाध्यायजी, यशपाल जैनजी, विष्णु प्रभाकरजी और सम्मान्य वियोगी हरिजी के दत्तक सुपुत्र भगवद्दत्त 'शिशु'जी की प्रियवार्ता होती रही और मैं मूक श्रोता ही बना रहा।
संयोग कुछ ऐसा बना कि सन् '74 में पिताजी को लोकनायक जयप्रकाशजी के आग्रह पर पटना छोड़ दिल्ली जाना पड़ा। कुछ महीने बाद, स्नातक की परीक्षा से निवृत्त होकर, मैं भी उन्हीं के पास पहुँच गया। दिल्ली की कई साहित्यिक सभाओं में विष्णु प्रभाकरजी के दर्शन और उनके व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त होता रहा, लेकिन वह दूर का दर्शन ही था। कभी-कदाचित् उन्हें प्रणाम निवेदित करने का अवसर भी मिल जाता था, लेकिन उनकी आँखों में मुझे अपने लिए अपरिचय का भाव ही अधिक दिखता। सन् '75 के अगस्त महीने में मैं अपनी पहली नौकरी पर कानपुर चला गया और उनकी निकटता पाने से वंचित रह गया।...
21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) के मीरापुर ग्राम में जन्मे विष्णु प्रभाकरजी से पिताजी की पुरानी मित्रता थी--आकाशवाणी सेवा-काल की, 1955-56 की, जब वह बतौर नाट्य-निर्देशक दिल्ली में सेवारत थे। वह पिताजी से दो-ढाई वर्ष छोटे थे और पिताजी को वयोज्येष्ठता का पूरा सम्मान देते थे। उनका आरम्भिक जीवन संघर्षपूर्ण था। उन्होंने बहुत परिश्रम और स्वप्रयत्न से अध्ययन किया था, उपाधियाँ अर्जित की थीं, भाषाएँ सीखी थीं और अंततः सन् '57 में सेवा-मुक्त होकर स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के रूप में चुना था। यह जोखिम-भरा निर्णय था, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहे और आजीवन लेखकीय दायित्वों का निर्वहन करते रहे। उन्होंने उत्कृष्ट गद्य-लेखन किया। वह गाँधीवादी युग के अप्रतिम रचनाकार थे। उनकी कृतियों में देश-प्रेम, राष्ट्रवाद और सामाजिक उत्थान की प्रबल भावना मुखरित हुई है।
कानपुर की नौकरी के दौरान ही मुझे विष्णु प्रभाकरजी के निकट आने तथा उनका स्नेहभाजन बनने का सुयोग प्राप्त हुआ था। स्वदेशी की सेवा के दौरान ही वहाँ मुझे मिले थे प्रभाकरजी के सुपुत्र--अमित भैया! लेकिन इसकी जानकारी मुझे बहुत बाद में हुई थी। वह मेरे खेल-मित्र थे और स्वदेशी के वरिष्ठ अधिकारी। हमारे बैचलर क्वार्टर के पीछे बने ऑफिसर्स क्वार्टर में सपत्नीक रहते थे। सुदर्शन युवा थे। उनसे सिर्फ क्लब में मिलना होता। मैं उनके साथ टेबल टेनिस खेलता। हमारी जोड़ी खूब जमती थी।
उन दिनों ही मैं अपने एक कृत्य के लिए बहुत प्रसिद्धि पा रहा था। वह कृत्य पराविलास था, जिसके लिए पिताजी की वर्जना मुझे मिलती रहती थी। एक दिन खेलकर हम दोनों पसीने-पसीने हुए कुर्सियों पर बैठ गए थे। थोड़े विश्राम के बाद घर जाते-जाते अमित भइया ने कहा--'मैं चार-पांच दिन क्लब नहीं आ सकूँगा। दिल्ली से मेरे माता-पिताजी आनेवाले हैं।' मैंने औपचारिकतावश उनसे पिताजी का नाम पूछ लिया। अमित भइया बोले--'वह जाने-माने साहित्यकार हैं। तुम तो हिंदी में रुचि रखते हो, तुमने उनका नाम अवश्य सुना होगा। उनका नाम है--श्रीविष्णु प्रभाकर।'
उनसे यह जानकार मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि वह स्वनामधन्य विष्णु प्रभाकरजी के सुपुत्र हैं। मैंने हुलसकर कहा--'वह तो मेरे पिताजी निकट मित्र हैं। १९७१ में उनसे मेरी एक मुलाकात भी हुई है--सस्ता साहित्य मण्डल कार्यालय में--कनॉट प्लेस में। संभव है, उन्हें इसका स्मरण न हो, लेकिन आप मेरे पिताजी का नाम लेंगे तो वह निश्चय ही पहचान लेंगे।'
अमित भाई ने मेरे पिताजी का नाम पूछा। मैंने पिताजी का पूरा नाम बताकर उनसे कहा--"आप उनसे सिर्फ 'मुक्तजी' कहेंगे तो भी वह पहचान लेंगे।"
इसके बाद दो दिन बीत गए। अमित भइया के क्लब में दर्शन न हुए। मैं समझ गया कि वह अपने माता-पिताजी के साथ व्यस्त होंगे। मेरे मन में यह इच्छा अवश्य थी कि एक बार फिर विष्णु प्रभाकरजी के दर्शन होते। दूसरे दिन शाम के वक़्त अमित भाई ने अपने सेवक को मेरे पास भेजा और सूचित किया कि पिताजी चाहते हैं, कल सुबह की चाय मैं उनके साथ पियूँ। मैं प्रफुल्लित हो उठा और सेवक से मैंने कल आने की स्वीकृति भेज दी।
सुबह तैयार होकर मैं पहली बार अमित भइया के घर पहुँचा। उस दिन विष्णु प्रभाकरजी से मिलकर परमानन्द हुआ। वह सौम्य-मूर्ति, संयत-सम्भाषी और अति स्नेही व्यक्ति थे। वह पिताजी का बड़े भाई की तरह बड़ा आदर-सम्मान करते थे। उस पीढ़ी के लोगों में आचार-व्यवहार की यह मानक परम्परा थी और लोग इसका पालन बहुत सावधानी से किया करते थे। यह पिताजी की घनिष्ठ मित्रता का ही प्रभाव था कि उस दिन वह बहुत प्रेम से मिले, पिताजी और मेरे काम-धंधे के बारे में पूछते रहे। इसी बीच अमित भाई बोल पड़े--'आनंद तो यहाँ बड़े साहस का काम कर रहे हैं। आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं।'
विष्णु प्रभाकरजी ने ठीक पिताजी की तरह ही मुझसे कहा था--"मनुष्य को प्रकाश की तरफ बढ़ाना चाहिए, अंधकार की ओर नहीं। परालोक एक अँधेरी सुरंग की तरह है और एक अँधेरी दुनिया में भटकने का कोई लाभ नहीं है। संभव है, इससे किसी का हित हो जाए, किसी को मनःशांति मिले, लेकिन किसी की हानि भी तो हो सकती है। इस दुविधापूर्ण दिशा में बढ़ने का क्या लाभ?'
मैं संकोच से गड़ा जा रहा था, शांत था; लेकिन चाहता था कि किसी तरह बात की दिशा बदल जाए। तभी बड़ा अच्छा हुआ कि श्रीमती प्रभाकर (पूजनीया चाचीजी) अपनी बहूजी के साथ चाय-नाश्ता लेकर आयीं। मैंने उनके चरण छुए और उनका आशीष पाकर धन्य हुआ। अब बात की दिशा स्वतः बदल गई थी। चाचीजी बहुत मृदुभाषिणी महिला थीं। उन्होंने आग्रहपूर्वक मुझे बहुत कुछ खिलाया और चाय पिलाई। जब चलने को हुआ तो बोलीं--'तुम मेस का भोजन करते हो न, कैसा खाना बनता है वहाँ?' मैंने कहा--'ठीक-ठाक, उदर-पूर्ति हो जाती है।'
मेरे उत्तर से उन्होंने जाने क्या अभिप्राय ग्रहण किया कि तत्काल मुझसे कहा--'तो ठीक है, आज रात का खाना तुम हमारे साथ ही कर रहे हो--घर का भोजन ! तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं वही बनाऊँगी, बोलो !' उनकी सहज और अनन्य प्रीति से मैं अभिभूत हो उठा था। मैंने कहा--'आप जो भी बनाएंगी, मैं प्रसन्नता से खाऊँगा।' उनकी ममतामयी मूर्ति देखकर और उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी।
अमित भइया के यहाँ रात के भोजन के वक़्त भी अमित आनंद हुआ। उन दिनों प्रभाकरजी की पुस्तक 'आवारा मसीहा' बहुत चर्चा में थी। वहाँ से परम तृप्त और आप्यायित हुआ जब लौटने लगा तो मैंने उनसे अपने लिए 'आवारा मसीहा' की एक प्रति मांगी तो बोले--'यहां तो प्रतियाँ हैं नहीं, तुम जब दिल्ली आओगे, तो उसकी प्रति तुम्हें अवश्य दूँगा। '
दो दिनों में श्रद्धेय विष्णु प्रभाकरजी के दो बार दर्शन पाकर और उनके सान्निध्य से मन बहुत प्रसन्न हुआ था, लेकिन उनकी वर्जना के शब्द कानों में निरंतर गूँज रहे थे--'मनुष्य को अन्धकार की ओर नहीं, प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए और…परालोक एक अँधेरी सुरंग की तरह है...!'
प्रख्यात साहित्यकार स्व. विष्णु प्रभाकरजी की जयन्ती पर सौभाग्य से मैं उनका स्नेहभाजन रहा हूं उन पर कुछ लिखने की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। जानता था, लिखने की बातें मेरे पास हैं, लेकिन यह स्मृति-लेख पूरा लिख न सका था। आज उस अकर्मण्ता से मुक्त होकर यह लंबा संस्मरण आप सबों के सामने रख रहा हूँ और इसी रूप में उनकी पावन स्मृतियों को स्मरण-नमन कर रहा हूँ।
(क्रमशः)