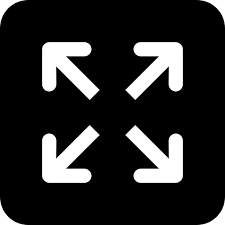TRENDING TAGS :
साल दर साल चुनाव का चूना
जब देश आजाद हुआ था तब हमारे रहनुमाओं ने यह उम्मीद की थी कि चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक पर्व होगा। लेकिन केवल वर्ष 1967 तक यह हो सका, इसके बाद तो बस चुनाव-पर्व सिर्फ परंपरा बन गया। देश के 28 राज्यों में शायद ही ऐसा कोई वर्ष होता होगा जिसमें दो तीन राज्यों में चुनाव न हों। शुरुआती दौर में तो हर साल चुनाव के चलन ने लोकतंत्र को थोड़ी गति, दिशा और मान्यता दी। लेकिन अब लोकतंत्र परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। हर साल चुनाव के चलन, लाभ हानि जोड़ा जाने लगा है, तबसे यह आवाज जोर पकड़ने लगी है कि अब बस। हर साल चुनाव का चलन बंद होना चाहिए। अब चुनाव के खर्चे इतने बढ़ गये हैं। आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। मसलन, 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 70 करोड़ रुपये सरकारी खर्च हुए। जबकि 2012 में यह राशि बढ़कर 200 करोड़ हो गयी। खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस एस ब्रह्मा ने यह माना है कि पांच साल के अंतराल के सभी राज्यो में चुनाव कराने का खर्च तकरीबन 4500 करोड़ रुपये आता है। उत्तर प्रदेश के साल 2102 के चुनाव में 350 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गये। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार के 3500 करोड़ रुपये खर्च। ये साल 2009 में हुए चुनावी खर्च का करीब 131 फीसदी था और पहले चुनाव यानी साल 1952 के चुनाव से 20 गुना कम था। 1952 में चुनावों पर कुल खर्च ही 10करोड़ हुआ था। दिलचस्प बात यह भी है कि 1952 में प्रति मतदाता चुनाव का खर्च महज 60 पैसे था वहीं साल 2014 में यह खर्च करीब 35 रुपये हो गया।
पिछले साल 2014 महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साल में कुछ महीनों के अंतराल में हुए। इस पर सरकार की ओर से 1100 करोड़ रुपये खर्च हुए। मई 2014 में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए वहीं महज 4 महीने बाद हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने सरकारी खजाने को 500 करोड़ की चपत लगाई। यानी तीन महीने की देरी ने जनता के 500 करोड़ स्वाहा करा दिए। इतना ही नहीं साल 2014 में ही हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव आम चुनाव 2014 के महज चार से 6 महीनों के भीतर ही हुए और करीब 1300 करोड़ का अतिरिक्त भार देश की जनता पर डाल गये। इस आर्थिक युग में निरंतर बढती यह आर्थिक मार अब बेवजह लगने लगी है।
सालाना चुनावी उत्सवों को अगर विकास के नज़रिए से भी देखा जाय तो नतीजे बेहद निराश करते हैं। हर राज्य में पांच साल में कम से कम तीन बार और ज्यादा से ज्यादा 6 बार चुनावी आचार संहिता में चक्कर में विकास के सभी कार्य ठप रहते हैं। आचार संहिता के चलते सरकार सिर्फ रुटीन काम निपटाती है। ऐसा नहीं है कि यह नज़रिया एकदम नया और बेवजह है। 1999 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी यह सलाह दी गयी है कि धीरे धीरे एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने की ओर बढ़ा जाना चाहिए। यही नहीं, एम एन वैंकट चलैया की अगुवाई में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। हाल फिलहाल, ई एम एस नचियप्पन की अगुवाई में न्याय संबंधी संसद की स्थाई समिति का गठन इसकी संभावना तलाशने में जुटी है। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से बातचीत के मार्फत तय समय पर एक साथ चुनाव की वकालत की दिशा में पांच साल पहले ही कदम बढ़ा दिया था।
हर साल चुनाव के चलते राजनैतिक दलों को हमेशा चुनाव के मूव और मूड में रहना पड़ता है। वर्ष 1967 से पहले जब एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव देश भर में होते थे तो लोकतंत्र महज उत्सव ही नहीं होता था। पर्व ही नहीं होता था। बल्कि, क्षेत्रीय क्षत्रपों की कुलांचे मारने वाली महत्वाकांक्षाओं को भी जनता का समर्थन हासिल नहीं हो पाता था। दस्तावेज चुगली करते हैं द्रमुक (1967), अन्नाद्रमुक (1973,1977), हविपा (1990), शिवसेना (1995), अकाली दल(1967), तेलगुदेशम(1984), राजद(1997), तृणमूल(1998), सपा(1994), बसपा(1994), रालोद(1996) आदि इत्यादि दलों का अभ्युदय 1967 के बाद ही हुआ। जब राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव होते हैं तो जनता के सामने मुद्दे, सवाल, समस्याएं और फलक भी राष्ट्रीय होते हैं। इन राष्ट्रीय विषयों पर ही हमारे राजनेताओं को अपने नीति और नीयत बतानी होती है। उन्हें देश की जनता को, समस्या को एड्रेस करना होता है। जब इलाकाई चुनाव होते हैं तो यह सब गौण हो जाता है। राष्ट्र और उससे जुड़ी समस्याएं इन क्षेत्रीय नेताओं के लिए बेमानी हो जाती हैं। देश में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने हमेशा राष्ट्रीय विकल्प बनने की कोशिश की पर इसमें राजनैतिक महात्वाकांक्षा ने हमेशा राष्ट्रीय भावना को दोयम दर्जे का बनाए रखा। नतीजा ये कि हर बार इस तरह के विकल्प जिसमें तीसरे चौथे मोर्चे की बात होती रही वह बनने से पहले ही व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा के दंश का शिकार हो गया। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्रीय क्षत्रप होगा जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो जिसका फलक, आयाम और दृष्टि राष्ट्रीय रहा हो। जिसने कभी पीएम की कुर्सी के अलावा कुछ सोचा हो। पीएम की कुर्सी तो सोच ली पर इन पीएम इन वेटिंग नेताओं की नज़र हमेशा राज्य की सीमाओं के बाहर निकलते ही धुंधली होती दिखती है। यही नहीं, इन समस्याओं के जगह जाति की जोड़ जुगत ले लेती है।
यही नहीं इतिहास साक्षी है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के उभार के बाद ही सियासत में वंशवाद और परिवार के बेल को खूब फलने फूलने का मौका मिला। डॉक्टर राममनोहर लोहिया का कांग्रेस के खिलाफ जंग का एक सबसे बड़ा हथियार वंशवाद होता था। वह गांधी नेहरू खानदान के खिलाफत का प्रतीक थे। लेकिन अब जब अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो यह मुद्दा बेमानी हो गया है। हद तो यह कि उनका नाम लेकर अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे उनके समाजवादियों के घर मे इस बेल में अपनी जड़ें कुछ ऐसे जमा ली हैं कि अब यह समाजवादी परिचय सा बन गया है। अगर जम्मू-कश्मीर से शुर करें तो कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, हिमाचल में प्रेमकुमार धूमल और वीरभद्र सिंह का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पुष्पित पल्लवित होती वंशबेल, बिहार में लालू राबडी का कुनबा, तमिलनाडु की पूरी राजनीति में द्रमुक अन्नाद्रमुक के वर्चस्व में एमजीआर से लेकर स्तालिन और कनिमोई तक का स्थापित कद। महाराष्ट्र में शिवसेना की पैतृक राजनीति का केंद्र और वंशवाद के लगातार फलते फूलते वटवृक्ष में रमन सिंह के पुत्र, दिग्विजय के कुंवर, राजनाथ के पंकज ने यह साबित कर दिया है कि वंशवाद अब बीमारी नहीं बल्कि पार्टियों की तासीर बन गयी है।
एक ऐसे समय जब राजनीति दो ध्रुवीय-राजग और संप्रग में कमोवेश बंटती हुई दिख रही हो तब तो एक साथ चुनाव का औचित्य और भी सिद्ध और साबित होता है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा की कद्र होनी चाहिए पर विचारधारा को हथियार बनाकर क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद को बढावा देन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया जब वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग हुए तब राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी विचारधारा वाले दल का विकल्प दिया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से बतौर उद्योग मंत्री पद से 6 अप्रैल को इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हुए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अंत्योदय की विचारधारा वाले एक दल को आकार दिया। ये बड़े नेता चाहते तो देश के किसी इलाके में अपना परचम उस तरह फहरा सकते थे जिस तरह आज का कोई क्षेत्रीय क्षत्रप फैला रहा है। पर इनके सपने बड़े थे। यह देश की चिंता करते थे। उन्हें विचारधारा के समानांतर एक विचारधारा देनी थी। वह कांग्रेस का विकल्प तैयार कर रहे थे। अपने लिए सत्ता और कुर्सी नहीं। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी कहा जा सकता है कि इन नेताओं में राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस का सामना करना था। नतीजतन उन्हें अपने फलक, नज़र और आयाम राष्ट्रीय रखने थे।
जब से राज्य और केंद्र के चुनाव अलग अलग होने लगे तब से यह नज़रिया, यह आयाम और यह फलक एकदम बदल गया। हद तो यह हुई कि क्षेत्रीय दलों के एजेंडे में आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा सिर्फ विरोध के लिए विरोध की तरह आया। विकास भी अपनी जाति तक ही सीमित होकर रह गया।यही नही एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति यह भी हुई कि काडर आधारित राजनीति का पराभव हो गया। विचारधारा राजनीति से शून्य हो गयी। महापुरुषों को जातिय स्तर पर बांट दिया गया। पार्टी का सिंबल बना दिया गया। उत्सव वाले चुनाव को प्रबंधन में तबदील कर दिया गया और ठेकेदार कार्यकर्ता हो गये। बाहुबली धनबली माननीय बन बैठे। चुनाव प्रचार एक इवेंट हो गया। नेता सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गया। चुनाव चेहरे पर होने लगे। यह सब पराभव के लक्षण हैं। ऐसे पराभव के लक्षण है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बहुत लोग यह कह सकते हैं कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो क्या होना चाहिए? क्या पांच साल इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन यह सवाल बेमानी क्योंकि जो भी सरकार गिराता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है उसको इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि वह वैकल्पिक नेता, वैकल्पिक सरकार पेश करे। वह नहीं कर पाता है तो लोकतंत्र में अस्थिरता के लिए उसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए।
खास बात ये है कि हर सर्वे हर रिपोर्ट हर शोध यही बताता है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के उदय के चलते ही देश में भ्रष्टाचार इस कदर बढा कि इस रैंकिंग में दुनिया के 93 देश हमसे ऊपर है। यानी हम ईमानदारी में दुनिया में 94वें स्थान पर हैं। इसे समझने के लिए किसी न्यूटन की साइंस समझने की जरुरत नही। सीधा समीकरण है कि हर पार्टी को चुनाव लडाना है। इसके लिए पार्टी छोटी हो या बडी उसे पैसा चाहिए। लगातार खर्चीले होते चुनाव की दौड़ में क्षेत्रीय छत्रप कहीं पिछड़ न जाएं इसके लिए भ्रष्टाचार का रास्ता सबसे सीधा शार्टकट है। लिहाजा सत्ता में आते ही विकास के बजाय क्षेत्रीय दलों का मकसद अगले चुनाव के लिए फंड जुटाना ही होता है। ऐसे में नेहरू-लोहिया यहां तक की जातिवादी राजनीति के जनक कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और नेहरू के बीच हुए पत्र व्यवहार जैसे उदाहरण, इस तरह का सृजनात्मक विपक्ष, बात व्यवहार, सुझाव अब बीते जमाने की आउटडेटेड बात बनकर रह गयी है। इस दौर में एक सवाल और जेरे-बहस होना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री और ग्राम प्रधान दोनों को पांच साल का समय क्यों। पंचायत और नगर निकाय चुनाव को भी लोकसभा और विधानसभा के साथ करा दिया जाय तो कल्पना कीजिए हमारी कितनी बचत होगी। देश का माहौल लोकतंत्र के उत्सव जैसा होगा। अलगाव वादी ताकतों के हौसले पस्त होंगे। बांटों और राज करो की नीति पराजित होगी। आदमी को वोटबैंक समझने की मंशा हारेगी।जातियों की ठेकेदारी खत्म होगी।
पिछले साल 2014 महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साल में कुछ महीनों के अंतराल में हुए। इस पर सरकार की ओर से 1100 करोड़ रुपये खर्च हुए। मई 2014 में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए वहीं महज 4 महीने बाद हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने सरकारी खजाने को 500 करोड़ की चपत लगाई। यानी तीन महीने की देरी ने जनता के 500 करोड़ स्वाहा करा दिए। इतना ही नहीं साल 2014 में ही हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव आम चुनाव 2014 के महज चार से 6 महीनों के भीतर ही हुए और करीब 1300 करोड़ का अतिरिक्त भार देश की जनता पर डाल गये। इस आर्थिक युग में निरंतर बढती यह आर्थिक मार अब बेवजह लगने लगी है।
सालाना चुनावी उत्सवों को अगर विकास के नज़रिए से भी देखा जाय तो नतीजे बेहद निराश करते हैं। हर राज्य में पांच साल में कम से कम तीन बार और ज्यादा से ज्यादा 6 बार चुनावी आचार संहिता में चक्कर में विकास के सभी कार्य ठप रहते हैं। आचार संहिता के चलते सरकार सिर्फ रुटीन काम निपटाती है। ऐसा नहीं है कि यह नज़रिया एकदम नया और बेवजह है। 1999 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी यह सलाह दी गयी है कि धीरे धीरे एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने की ओर बढ़ा जाना चाहिए। यही नहीं, एम एन वैंकट चलैया की अगुवाई में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। हाल फिलहाल, ई एम एस नचियप्पन की अगुवाई में न्याय संबंधी संसद की स्थाई समिति का गठन इसकी संभावना तलाशने में जुटी है। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से बातचीत के मार्फत तय समय पर एक साथ चुनाव की वकालत की दिशा में पांच साल पहले ही कदम बढ़ा दिया था।
हर साल चुनाव के चलते राजनैतिक दलों को हमेशा चुनाव के मूव और मूड में रहना पड़ता है। वर्ष 1967 से पहले जब एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव देश भर में होते थे तो लोकतंत्र महज उत्सव ही नहीं होता था। पर्व ही नहीं होता था। बल्कि, क्षेत्रीय क्षत्रपों की कुलांचे मारने वाली महत्वाकांक्षाओं को भी जनता का समर्थन हासिल नहीं हो पाता था। दस्तावेज चुगली करते हैं द्रमुक (1967), अन्नाद्रमुक (1973,1977), हविपा (1990), शिवसेना (1995), अकाली दल(1967), तेलगुदेशम(1984), राजद(1997), तृणमूल(1998), सपा(1994), बसपा(1994), रालोद(1996) आदि इत्यादि दलों का अभ्युदय 1967 के बाद ही हुआ। जब राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव होते हैं तो जनता के सामने मुद्दे, सवाल, समस्याएं और फलक भी राष्ट्रीय होते हैं। इन राष्ट्रीय विषयों पर ही हमारे राजनेताओं को अपने नीति और नीयत बतानी होती है। उन्हें देश की जनता को, समस्या को एड्रेस करना होता है। जब इलाकाई चुनाव होते हैं तो यह सब गौण हो जाता है। राष्ट्र और उससे जुड़ी समस्याएं इन क्षेत्रीय नेताओं के लिए बेमानी हो जाती हैं। देश में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने हमेशा राष्ट्रीय विकल्प बनने की कोशिश की पर इसमें राजनैतिक महात्वाकांक्षा ने हमेशा राष्ट्रीय भावना को दोयम दर्जे का बनाए रखा। नतीजा ये कि हर बार इस तरह के विकल्प जिसमें तीसरे चौथे मोर्चे की बात होती रही वह बनने से पहले ही व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा के दंश का शिकार हो गया। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्रीय क्षत्रप होगा जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो जिसका फलक, आयाम और दृष्टि राष्ट्रीय रहा हो। जिसने कभी पीएम की कुर्सी के अलावा कुछ सोचा हो। पीएम की कुर्सी तो सोच ली पर इन पीएम इन वेटिंग नेताओं की नज़र हमेशा राज्य की सीमाओं के बाहर निकलते ही धुंधली होती दिखती है। यही नहीं, इन समस्याओं के जगह जाति की जोड़ जुगत ले लेती है।
यही नहीं इतिहास साक्षी है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के उभार के बाद ही सियासत में वंशवाद और परिवार के बेल को खूब फलने फूलने का मौका मिला। डॉक्टर राममनोहर लोहिया का कांग्रेस के खिलाफ जंग का एक सबसे बड़ा हथियार वंशवाद होता था। वह गांधी नेहरू खानदान के खिलाफत का प्रतीक थे। लेकिन अब जब अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो यह मुद्दा बेमानी हो गया है। हद तो यह कि उनका नाम लेकर अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे उनके समाजवादियों के घर मे इस बेल में अपनी जड़ें कुछ ऐसे जमा ली हैं कि अब यह समाजवादी परिचय सा बन गया है। अगर जम्मू-कश्मीर से शुर करें तो कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, हिमाचल में प्रेमकुमार धूमल और वीरभद्र सिंह का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पुष्पित पल्लवित होती वंशबेल, बिहार में लालू राबडी का कुनबा, तमिलनाडु की पूरी राजनीति में द्रमुक अन्नाद्रमुक के वर्चस्व में एमजीआर से लेकर स्तालिन और कनिमोई तक का स्थापित कद। महाराष्ट्र में शिवसेना की पैतृक राजनीति का केंद्र और वंशवाद के लगातार फलते फूलते वटवृक्ष में रमन सिंह के पुत्र, दिग्विजय के कुंवर, राजनाथ के पंकज ने यह साबित कर दिया है कि वंशवाद अब बीमारी नहीं बल्कि पार्टियों की तासीर बन गयी है।
एक ऐसे समय जब राजनीति दो ध्रुवीय-राजग और संप्रग में कमोवेश बंटती हुई दिख रही हो तब तो एक साथ चुनाव का औचित्य और भी सिद्ध और साबित होता है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा की कद्र होनी चाहिए पर विचारधारा को हथियार बनाकर क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद को बढावा देन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया जब वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग हुए तब राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी विचारधारा वाले दल का विकल्प दिया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से बतौर उद्योग मंत्री पद से 6 अप्रैल को इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हुए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अंत्योदय की विचारधारा वाले एक दल को आकार दिया। ये बड़े नेता चाहते तो देश के किसी इलाके में अपना परचम उस तरह फहरा सकते थे जिस तरह आज का कोई क्षेत्रीय क्षत्रप फैला रहा है। पर इनके सपने बड़े थे। यह देश की चिंता करते थे। उन्हें विचारधारा के समानांतर एक विचारधारा देनी थी। वह कांग्रेस का विकल्प तैयार कर रहे थे। अपने लिए सत्ता और कुर्सी नहीं। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी कहा जा सकता है कि इन नेताओं में राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस का सामना करना था। नतीजतन उन्हें अपने फलक, नज़र और आयाम राष्ट्रीय रखने थे।
जब से राज्य और केंद्र के चुनाव अलग अलग होने लगे तब से यह नज़रिया, यह आयाम और यह फलक एकदम बदल गया। हद तो यह हुई कि क्षेत्रीय दलों के एजेंडे में आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा सिर्फ विरोध के लिए विरोध की तरह आया। विकास भी अपनी जाति तक ही सीमित होकर रह गया।यही नही एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति यह भी हुई कि काडर आधारित राजनीति का पराभव हो गया। विचारधारा राजनीति से शून्य हो गयी। महापुरुषों को जातिय स्तर पर बांट दिया गया। पार्टी का सिंबल बना दिया गया। उत्सव वाले चुनाव को प्रबंधन में तबदील कर दिया गया और ठेकेदार कार्यकर्ता हो गये। बाहुबली धनबली माननीय बन बैठे। चुनाव प्रचार एक इवेंट हो गया। नेता सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गया। चुनाव चेहरे पर होने लगे। यह सब पराभव के लक्षण हैं। ऐसे पराभव के लक्षण है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बहुत लोग यह कह सकते हैं कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो क्या होना चाहिए? क्या पांच साल इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन यह सवाल बेमानी क्योंकि जो भी सरकार गिराता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है उसको इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि वह वैकल्पिक नेता, वैकल्पिक सरकार पेश करे। वह नहीं कर पाता है तो लोकतंत्र में अस्थिरता के लिए उसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए।
खास बात ये है कि हर सर्वे हर रिपोर्ट हर शोध यही बताता है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के उदय के चलते ही देश में भ्रष्टाचार इस कदर बढा कि इस रैंकिंग में दुनिया के 93 देश हमसे ऊपर है। यानी हम ईमानदारी में दुनिया में 94वें स्थान पर हैं। इसे समझने के लिए किसी न्यूटन की साइंस समझने की जरुरत नही। सीधा समीकरण है कि हर पार्टी को चुनाव लडाना है। इसके लिए पार्टी छोटी हो या बडी उसे पैसा चाहिए। लगातार खर्चीले होते चुनाव की दौड़ में क्षेत्रीय छत्रप कहीं पिछड़ न जाएं इसके लिए भ्रष्टाचार का रास्ता सबसे सीधा शार्टकट है। लिहाजा सत्ता में आते ही विकास के बजाय क्षेत्रीय दलों का मकसद अगले चुनाव के लिए फंड जुटाना ही होता है। ऐसे में नेहरू-लोहिया यहां तक की जातिवादी राजनीति के जनक कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और नेहरू के बीच हुए पत्र व्यवहार जैसे उदाहरण, इस तरह का सृजनात्मक विपक्ष, बात व्यवहार, सुझाव अब बीते जमाने की आउटडेटेड बात बनकर रह गयी है। इस दौर में एक सवाल और जेरे-बहस होना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री और ग्राम प्रधान दोनों को पांच साल का समय क्यों। पंचायत और नगर निकाय चुनाव को भी लोकसभा और विधानसभा के साथ करा दिया जाय तो कल्पना कीजिए हमारी कितनी बचत होगी। देश का माहौल लोकतंत्र के उत्सव जैसा होगा। अलगाव वादी ताकतों के हौसले पस्त होंगे। बांटों और राज करो की नीति पराजित होगी। आदमी को वोटबैंक समझने की मंशा हारेगी।जातियों की ठेकेदारी खत्म होगी।
Next Story