TRENDING TAGS :
‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’- राष्ट्रकवि दिनकर
हिन्दी के सुविख्यात कवि रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ई. में सिमरिया, ज़िला मुंगेर (बिहार) में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा
राष्ट्रकवि दिनकरजी की 109वीं जयन्ती (23 सितम्बर) पर पुण्य-स्मरण
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो – (कुरूक्षेत्र से)
‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’
लखनऊ: हिन्दी के सुविख्यात कवि रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ई. में सिमरिया, ज़िला मुंगेर (बिहार) में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मन रूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। गाँव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडल स्कूल में प्रवेश प्राप्त किया। 1928 में मैट्रिक के बाद, दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बी. ए. ऑनर्स किया। अगले ही वर्ष एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब-रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग नौ वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्वगीत उनके द्वारा रचे गए।
रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाऐं यहां-वहां प्रकाश में आईं और अग्रेज़ प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक ग़लत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं। और दिनकर की फ़ाइल तैयार होने लगी, बात-बात पर क़ैफ़ियत तलब होती और चेतावनियां मिला करतीं। चार वर्ष में बाईस बार उनका तबादला किया गया।
1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद-सदस्य रहे, बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ई. तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ई. तक अपना हिन्दी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए।
क्रांतिकारी कवि
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नयी ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया।
इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था।
दिनकर का पहला काव्यसंग्रह ‘विजय संदेश’ वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ‘परशुराम की प्रतीक्षा’, ‘हुंकार’ और ‘उर्वशी’ हैं. उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया
एक अदद 'न' का ही तो सवाल था
 'अन्वेषी आँखें'...'आत्मा की आँखें'...
'अन्वेषी आँखें'...'आत्मा की आँखें'...
राष्ट्रकवि पूज्य दिनकरजी के कक्ष में, उनकी कृपा-छाया में, उनके दिशा-निर्देश में, उनके श्रीचरणों में बैठकर डेढ़ महीने तक सेवा-भावना से उन्हीं का काम करना अपूर्व सुखदायक था। वे डेढ़ महीने जीवन के अविस्मरणीय दिन थे। मैंने बहुत कुछ सीखा था उनसे, बहुत-से प्रसंग सुने और अनेक कविताएँ सुनी थीं उनके श्रीमुख से। उन्हीं दिनों का एक वाकया याद आता है।
अपने काॅलेज से छूटकर उस दिन (1-5-1972 ) भी मैं यथासमय दिनकरजी के घर पहुँच गया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे बारह बजे तक लौट जाना था। यह बात मैंने उन्हें बतायी तो बोले--'हाँ-हाँ, जरूर जाओ। डेढ़-दो घण्टे में जितना हो सके, उतना ही काम करो।' फिर मैं काम में जुट गया। 'दिनकर की डायरी' की पाण्डुलिपि के जितने पृष्ठ लिखने संभव थे, मैंने बारह बजे तक लिखे। बारह बजते ही मैं जाने को उठ खड़ा हुआ। उस वक्त दिनकरजी स्नानघर में जाने के लिए अपने वस्त्र उठा रहे थे।
मैंने उनसे कहा--'चाचाजी! बारह बज गये, अब मैं जाता हूँ।'
उन्होंने स्वीकृति दी और मैंने लौट चलने को कदम बढ़ाये ही थे कि जाने उन्हें क्या सूझी, उन्होंने कहा--'ठहरो!'
मेरे बढ़ते कदम ठिठक गये। मैं पलटा और उनकी ओर मुखातिब हुआ। मैंने देखा, वह अपने हाथ में उठाया हुआ वस्त्र कुर्सी के हत्थे पर रखकर अलमारी में सजी किताबों के पास गये और एक पुस्तक निकाल लाये। वह उनकी काव्य-पुस्तिका 'आत्मा की आँखें' थी। अपनी कलम से उसकी जिल्द के बादवाले पृष्ठ पर उन्होंने कुछ लिखा और मुझे देते हुए बोले--'लो, इसे पढ़ना। यह 'मुक्त' के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है।'
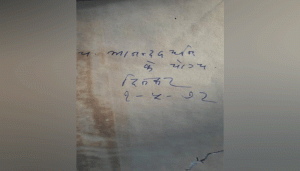
मैं उपकृत हुआ। पुस्तक को मैंने सिर से लगाया, अपने कंधे से लटकते बुद्धिजीवी झोले में रखा और वापस लौट चला। दिनकरजी के घर से लंबी पद-यात्रा करके मुख्य सड़क पर आना होता था, जहाँ से कोई वाहन मिलता था और वह मुझे मेरे घर पटनासिटी तक पहुँचा देता था। दिनकरजी के राजेन्द्र नगरवाले घर से निकलकर मैं क्षिप्रता से चलने लगा। अभी दो-तीन फर्लांग ही गया होऊँगा कि मन में यह जानने का लोभ उत्पन्न हुआ कि देखूँ, दिनकरजी ने पुस्तक पर आखिर लिखा क्या है? इस विचार के मन में उपजते ही मेरी गति शिथिल हुई। मैंने झोले से पुस्तक निकाली, जिल्द पलटकर दिनकरजी की लिखित पंक्ति पढ़ने लगा। उन्होंने लिखा था--
"चि. आनन्द वर्ध
के योग्य,
--दिनकर
1-5-1972."
'वर्धन' का अंतिम अक्षर 'न' लिखने से रह गया था। मुझे घर पहुँचने की जल्दबाजी थी, फिर भी मैं उलटे पाँव लौटा। दिनकरजी के घर पहुँचा तो पाया, वह स्नानागार में हैं। मैं उनके कक्ष में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में वह बाहर आये और मुझे देखते ही बोल पड़े--'अरे, तुम लौट क्यों आये?'
मैंने संकुचित भाव से कहा--"एक 'न' छूट गया है, इसलिए!" वह अभिप्राय कुछ समझ न सके। उन्होंने फिर पूछा--'क्या कहा?'
अब और कुछ कहना मेरे लिए कठिन था। मैंने पुस्तक की जिल्द खोलकर उनके सामने कर दी, बोला कुछ नहीं। उन्होंने पृष्ठ पर दृष्टिपात न करके मुझसे कहा--'हां, यह पुस्तक मैंने दी है तुम्हें!'..
अपनी बात स्पष्टतः उनके सामने रखना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था मुझे ! अंततः पृष्ठ की ओर इंगित करते हए मैंने कहा--'आपने जो लिखा है, उसे पढ़िये।' वह अपने लिखे को पढ़ने लगे और हठात् ठहाका मारकर हँस पड़े। जब संयत हुए तो बोले--"एक अदद 'न' का ही तो सवाल था! इसे तो तुम कल भी लिखवा सकते थे मुझसे। दूर तक जाकर लौट आने की क्या आवश्यकता थी?"
उन्होंने कलम उठायी और यथास्थान 'न' लिखा दिया और पुस्तक मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले--'अब इस उम्र में मुझसे ऐसी गफ़लत होने लगी है। पहले ऐसा न था।'
मैं चलने लगा तो दिनकरजी ने खड़े होकर मेरी पीठ थपथपाई और कहा--"लगता है, अशुद्धियों-कमियों को परास्त करने का यह विरल गुण तुमने मुक्तजी से ही ग्रहण किया है। उनके सुपुत्र की ऐसी ही 'अन्वेषी आंखें' होनी चाहिए।"...
तीन लघ्वाकार पंक्तियों में एकमात्र शब्द की छूट की औचक पकड़ में मैंने कोई भगीरथ प्रयत्न नहीं किया था। अतिउत्सुकता में राह चलते पुस्तक की जिल्द पलटी और तीनों पंक्तियाँ पढ़ डालीं। दूसरी पंक्ति में अपने नाम पर पहुँचते ही आँखें ठिठक गयी थीं। मैं उल्टे पाँव लौटा था। इसमें मेरी पात्रता अथवा महार्घता का प्रश्न ही कहां था, लेकिन विपथ हुए एक अदद 'न' को राह पर ले आने की ऐसी तत्परता की इतनी मुखर प्रशंसा, इस रूप में, राष्ट्रकवि दिनकरजी से ही मिल सकती थी। यह उनका अमोघ आशीर्वाद ही था, जिसे ग्रहण कर और विनयपूर्वक उन्हेंं प्रणाम कर मैंं प्रसन्नचित्त घर लौटा।...
व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने
व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने !
भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं,
उड़ न सकते हम धुमैले स्वप्न तक,
शक्ति हो तो आ, बसा अलका यहीं।
फूल से सज्जित तुम्हारे अंग हैं
और हीरक-ओस का श्रृंगार है,
धूल में तरुणी-तरुण हम रो रहे,
वेदना का शीश पर गुरु भार है।
अरुण की आभा तुम्हारे देश में,
है सुना, उसकी अमिट मुसकान है;
टकटकी मेरी क्षितिज पर है लगी,
निशि गई, हँसता न स्वर्ण-विहान है।
व्योम-कुंजों की सखी, अयि कल्पने !
आज तो हँस लो जरा वनफूल में
रेणुके ! हँसने लगे जुगनू, चलो,
आज कूकें खँडहरों की धूल में।






